Avyay Ki Paribhasha
अव्यय (Avyay) वे शब्द हैं जो अपरिवर्तनीय होते हैं, यानी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के विपरीत, ये किसी भी लिंग, वचन, पुरुष या काल के आधार पर नहीं बदलते। अव्यय स्थिर और अपरिवर्तित रहते हैं, इसीलिए इन्हें ‘अविकारी शब्द’ कहा जाता है। उदाहरण के लिए, शब्द जैसे—जब, तब, किन्तु, परन्तु, इधर, उधर, अभी, अतएव, क्योंकि, इत्यादि—समय, स्थान, या कारण के संदर्भ में ही अपनी स्थिति स्पष्ट करते हैं, परंतु स्वरूप में बदलाव नहीं लाते।
अव्यय के भेद (Avyay Ke Bhed)
अव्यय Avyay चार प्रकार के होते हैं-
(क) क्रिया विशेषण (Kriya Visheshan)
(ख) सम्बन्ध बोधक अव्यय (Sambandhabodhak Avyay)
(ग) समुच्चय बोधक अव्यय (Vismayadibodhak Avyay)
(घ) विस्मयादि बोधक अव्यय (Vismayadibodhak Avya)
(ड़) निपात (Nipat)
(क) क्रिया विशेषण: एक विश्लेषण (Kriya Visheshan)
वे शब्द जो किसी क्रिया की विशेषता को दर्शाते हैं, उन्हें “क्रिया विशेषण” कहते हैं। उदाहरणस्वरूप:
- “वह वहाँ टहलता है।” (यहाँ ‘वहाँ’ शब्द उस स्थान का संकेत देता है जहाँ वह टहल रहा है।)
- “मैं इधर देखता हूँ।” (यहाँ ‘इधर’ शब्द उस दिशा को प्रकट करता है जहाँ देख रहा हूँ।)
उदाहरण स्वरूप:
- साहिल रोज़ स्कूल जाता है। (यहाँ ‘रोज़’ शब्द क्रिया ‘जाता है’ की समय-संबंधी विशेषता को दर्शाता है।)
- लड़का ज़ोर से चिल्लाता है। (‘ज़ोर’ शब्द चिल्लाने की तीव्रता को प्रकट करता है।)
- चील ने नीचे देखा। (‘नीचे’ शब्द क्रिया ‘देखा’ का स्थान बताता है।)
क्रिया विशेषण के भेद
क्रिया विशेषण विभिन्न रूपों में होते हैं, जिनमें प्रयोग, रूप, और अर्थ के अनुसार भिन्नताएँ हैं। आइए इन्हें विस्तार से समझते हैं।
1. प्रयोग के अनुसार विभाजन
साधारण क्रियाविशेषण अव्यय – ऐसे शब्द जो स्वतंत्र रूप से वाक्य में प्रयुक्त होते हैं।
- उदाहरण: “हाय! मैं क्या करूँ।” (यहाँ ‘हाय’ भाव का संकेत है।)
संयोजक क्रियाविशेषण अव्यय – ऐसे शब्द जिनका संबंध उपवाक्य से होता है।
- उदाहरण: “जहाँ समुद्र है, वहाँ कभी जंगल था।” (‘जहाँ’ शब्द स्थान का संकेत देता है।)
अनुबद्ध क्रियाविशेषण अव्यय – निश्चय का संकेत देते हैं।
- उदाहरण: “मैंने उसे देखा तक नहीं।” (‘तक’ शब्द यहाँ विशेष ध्यानाकर्षण की भूमिका निभाता है।)
2. रूप के अनुसार विभाजन
मूल क्रियाविशेषण अव्यय – जिनमें किसी और शब्द का मेल नहीं होता।
- उदाहरण: “अचानक से सांप आ गया।” (‘अचानक’ बिना किसी अन्य शब्द की आवश्यकता के अपनी स्थिति प्रकट करता है।)
यौगिक क्रियाविशेषण अव्यय – जिनमें दूसरे शब्दों का मेल होता है।
- उदाहरण: “वह रातभर जागता रहा।” (‘रातभर’ समय का संकेत देता है।)
स्थानीय क्रियाविशेषण अव्यय – जो स्थान का संकेत देते हैं।
- उदाहरण: “वह नीचे बैठा है।” (‘नीचे’ विशेष स्थान का संकेत है।)
3. अर्थ के अनुसार भेद
कालवाचक क्रियाविशेषण अव्यय – समय का संकेत देते हैं।
- उदाहरण: “मैं आज स्कूल गया।” (‘आज’ शब्द समय बतलाता है।)
स्थानवाचक क्रियाविशेषण अव्यय – स्थान को प्रकट करते हैं।
- उदाहरण: “वह इधर-उधर देख रहा था।” (‘इधर-उधर’ से दिशा का पता चलता है।)
परिमाणवाचक क्रियाविशेषण अव्यय – कार्य की तीव्रता या मात्रा का संकेत देते हैं।
- उदाहरण: “वह बहुत तेज़ दौड़ता है।” (‘बहुत’ से गति का बोध होता है।)
रीतिवाचक क्रियाविशेषण अव्यय – कार्य करने के तरीके या शैली का संकेत देते हैं।
- उदाहरण: “वह ध्यानपूर्वक काम करता है।” (‘ध्यानपूर्वक’ कार्य की विधि का संकेत है।)
संख्यावाचक क्रियाविशेषण – संख्या का ज्ञान देते हैं।
- उदाहरण: “मैं यह किताब दो बार पढ़ चुका हूँ।” (‘दो बार’ पढ़ने की संख्या को दर्शाता है।)
स्वीकार वाचक – क्रिया के प्रति स्वीकृति प्रकट करते हैं।
- उदाहरण: “हाँ, मैं जाऊँगा।” (‘हाँ’ स्वीकृति को दर्शाता है।)
निषेध वाचक – क्रिया के निषेध का संकेत देते हैं।
प्रश्नवाचक क्रियाविशेषण – प्रश्न की स्थिति को दर्शाते हैं।
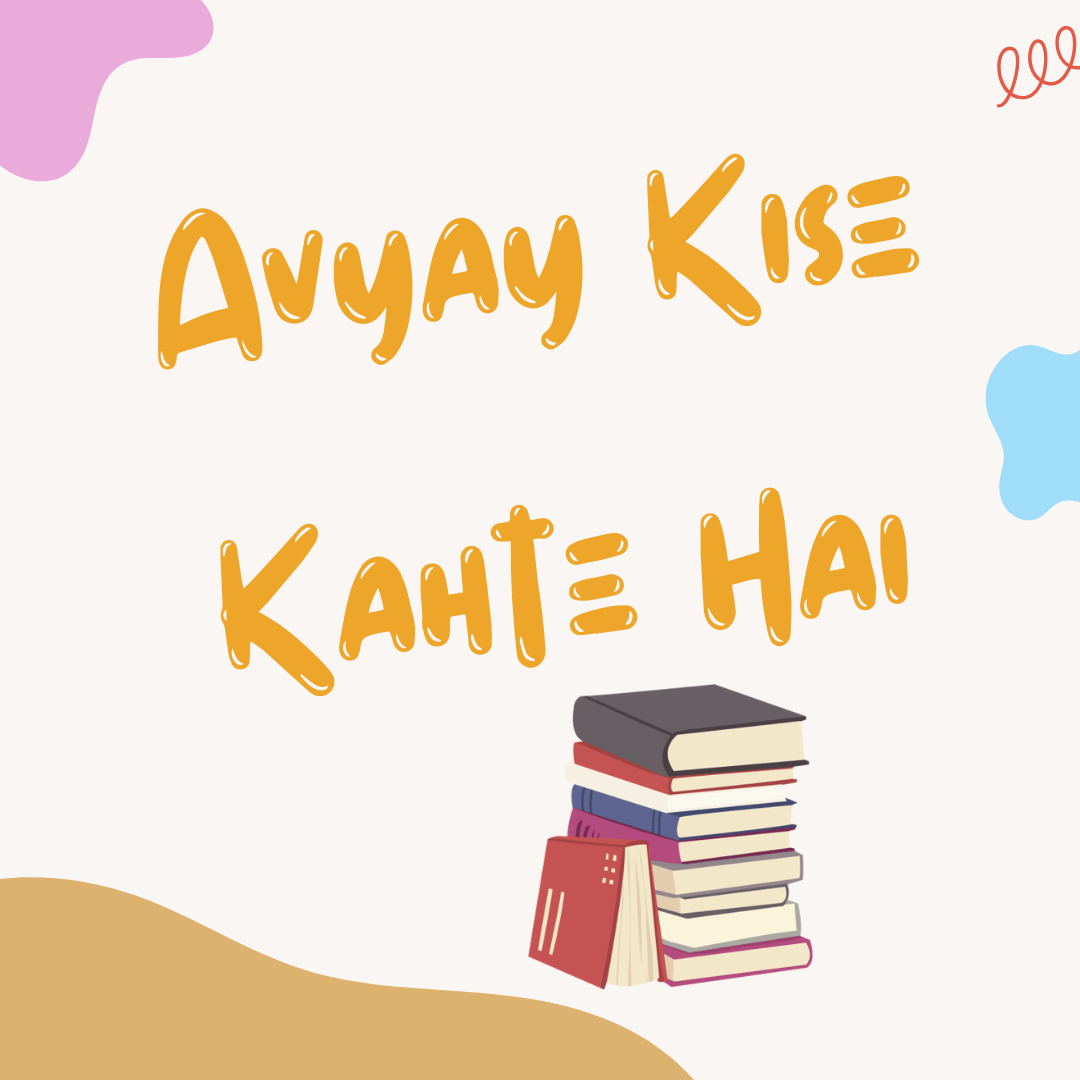
(ख) सम्बन्धबोधक अव्यय (Sambandhabodhak Avyay)
अव्यय (Avyay) शब्दों का एक विशेष वर्ग होता है, जिनसे संज्ञा या सर्वनाम के अन्य शब्दों से सम्बंध स्पष्ट होता है। इन शब्दों को ही सम्बन्धबोधक अव्यय Avyay कहा जाता है। यह अव्यय कई प्रकारों में विभाजित किए गए हैं, जो अर्थ के अनुसार अलग-अलग हैं:
- कालवाचक – यह समय का बोध कराते हैं। जैसे: पहले, बाद, ओग, पीछे।
- स्थानवाचक – ये स्थान का संकेत करते हैं। जैसे: बाहर, भीतर, बीच, ऊपर, नीचे।
- दिशावाचक – दिशा को व्यक्त करने वाले अव्यय। जैसे: निकट, पास, समीप, ओर, सामने।
- साधनवाचक – साधन या माध्यम को व्यक्त करते हैं। जैसे: निमित्त, द्वारा, जरिये।
- विरोधवाचक – विरोधाभास को प्रकट करते हैं। जैसे: उलटे, विरूद्ध, प्रतिकूल।
- व्यतिकवाचक – इनमें अपवाद का भाव रहता है। जैसे: सिवा, अलावा, बिना, बगैर, अतिरिक्त, रहित।
- उद्देश्यवाचक – उद्देश्य के लिए प्रयुक्त। जैसे: लिए, वास्ते, हेतु, निमित्त।
- साचर्यवाचक – साथ का संकेत देने वाले। जैसे: समेत, संग, साथ, सहित।
- विशयवाचक – विषय से सम्बंधित। जैसे: विषय, बाबत, लेख।
- संग्रहवाचक – संग्रह या समावेश का संकेत। जैसे: समेत, भर, तक।
- विनिमयवाचक – विनिमय का भाव। जैसे: बदले, जगह, एवज।
- सादृश्यवाचक – समानता का भाव। जैसे: समान, तरह, भाँति, नाई।
- तुलनावाचक – तुलना का संकेत। जैसे: अपेक्षा, वनस्पित, आगे, सामने।
- कारणवाचक – कारण को दर्शाते हैं। जैसे: कारण, परेशानी से, मारे।
प्रयोग और भेद
सम्बन्धबोधक अव्यय के तीन प्रमुख भेद हैं:
- सविभक्तिक: ये अव्यय विभक्ति के साथ प्रयुक्त होते हैं। जैसे, आगे, पीछे, समीप आदि।
- निर्विभक्तिक: ये अव्यय बिना विभक्ति के प्रयोग होते हैं। जैसे, भर, तक, समेत आदि।
- उभय विभक्ति: ये अव्यय विभक्ति के साथ और बिना विभक्ति के, दोनों प्रकार से प्रयुक्त होते हैं। जैसे, द्वारा, रहित, बिना, अनुसार आदि।
क्रियाविशेषण और सम्बन्धबोधक अव्यय में अंतर
यदि इन अव्ययों का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के साथ हो, तो ये सम्बन्धबोधक होते हैं। लेकिन जब इन्हें क्रिया के विशेषण के रूप में उपयोग किया जाता है, तो इन्हें क्रियाविशेषण कहा जाता है।
(ग) समुच्चय बोधक अव्यय (Samuchchay Bodhak Avyay)
समुच्चयबोधक अव्यय Avyay, जिनका काम दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ना होता है, का एक खास स्थान है। ये शब्द हमें वाक्यों में एक तारतम्य का अनुभव कराते हैं और इसीलिए इन्हें ‘योजक’ भी कहते हैं। समुच्चयबोधक अव्ययों के तीन प्रमुख प्रकार होते हैं—संयोजक, विभाजक, और विकल्पसूचक।
1. संयोजक
संयोजक वे अव्यय Avyay हैं जो दो या अधिक शब्दों या वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं, जिससे वे एक विचार या भाव के रूप में संगठित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए: “और,” “एवं,” “व” जैसे शब्द।
उदाहरण:
- “मैं और राम काम पर जाएँगे।”
- “राम, लक्ष्मण और सीता ने पंचवटी में विश्राम किया।”
इन वाक्यों में “और,” “एवं,” “तथा” जैसे शब्द सीधे तौर पर जोड़ने का कार्य करते हैं। ये सिर्फ शब्दों को नहीं, बल्कि उनके पीछे के भावों को भी एक सूत्र में पिरोते हैं।
2. विभाजक
विभाजक अव्यय वो होते हैं जो दो या दो से अधिक विकल्पों में से एक को चुनने या त्यागने की स्थिति बताते हैं। इनका उद्देश्य किसी एक विकल्प की ओर इंगित करना होता है। कुछ सामान्य विभाजक हैं—“किन्तु,” “परन्तु,” “अगर,” “ताकि,” “क्योंकि,” “इसलिए।”
उदाहरण:
- “करो या मरो।”
- “नित्य आराम करो ताकि स्वस्थ रहो।”
यहाँ “या” और “ताकि” जैसे शब्द भिन्नता को दिखाते हुए जुड़ने का काम करते हैं, जिससे एक स्पष्ट अर्थ का संचार होता है।
3. विकल्पसूचक
विकल्पसूचक अव्यय, जो विकल्प की स्थिति को दर्शाते हैं, किसी स्थिति या कार्रवाई में विभिन्न संभावनाओं को व्यक्त करते हैं। इनके कुछ उदाहरण हैं—“या,” “अन्यथा,” “अथवा,” “न कि।”
उदाहरण:
- “तुम आना या मैं आऊँगा।”
- “तुम पैसे का प्रबंध कर लो, अन्यथा मुझे कुछ और करना पड़ेगा।”
यहाँ पर “या” और “अन्यथा” जैसे शब्द विकल्पों को प्रस्तुत करते हैं, जो परिस्थिति को और भी रोचक बनाते हैं।
समुच्चयबोधक अव्ययों का यह विभाजन भाषा को अधिक प्रभावी बनाता है, जिससे हम विभिन्न विचारों को एक संगठित और सार्थक ढंग से जोड़ने में सक्षम हो पाते हैं।
(घ) विस्मयादिबोधक अव्यय (Vismayadibodhak Avyay)
वे शब्द, जो मनुष्य के हर्ष, शोक, विस्मय, तिरस्कार, या स्वीकृति जैसे भावों को व्यक्त करते हैं, विस्मयादिबोधक अव्यय Avyay कहलाते हैं। इन शब्दों का उद्देश्य हमारे मन के विभिन्न भावों को बिना किसी अतिरिक्त विवरण के सामने लाना होता है। इन्हें भावों के प्रतीक, ‘द्योतक’, भी कहते हैं। भाव की गहराई के अनुसार, विस्मयादिबोधक अव्यय के विभिन्न प्रकार होते हैं:
- हर्षबोधक – जब हृदय में खुशी और उत्साह उमड़ता है, तो हम कहते हैं: “अहा!,” “धन्य!,” “वाह-वाह!,” “वाह!,” “शाबाश!”। ये शब्द केवल हर्ष का भाव ही नहीं, बल्कि उसके साथ ऊर्जा और उमंग भी प्रकट करते हैं।
- शोकबोधक – दुःख के क्षणों में, शब्द निकलते हैं: “आह!,” “हाय!,” “हाय-हाय!,” “हा!,” “त्राहि-त्राहि!” या “बाप रे!”। इनमें एक अनकही पीड़ा और क्षोभ छिपा होता है जो सीधे दिल को छू जाता है।
- विस्मयबोधक – विस्मय और चकित कर देने वाली बातों पर, हम चौंकते हैं: “हैं!” “ऐं!” “ओहो!” “अरे!” “वाह!”। ये शब्द अचानक की गई खोज या अप्रत्याशित घटना पर गहरी प्रतिक्रिया देते हैं।
- तिरस्कारबोधक – अवमानना या निराशा के पलों में, हम तिरस्कार से कहते हैं: “छिः,” “हट!” “धिक!,” “धत्!,” “छि छिः!” और “चुप!”। इन शब्दों में क्रोध या घृणा की तीव्रता छिपी होती है।
- स्वीकृतिबोधक – सहमति या अनुमोदन में, हम सहजता से कहते हैं: “हाँ-हाँ!,” “अच्छा!,” “ठीक!,” “जी हाँ!,” “बहुत अच्छा!”। यह स्वीकृति का भाव न केवल संपूर्णता में बल्कि शांति और संतोष का भी संकेत देता है।
- सम्बोधनबोधक – संबोधन करते समय, हमारे शब्द बन जाते हैं: “रे!” “री!” “अरे!” “अरी!” “ओ!” “अजी!” “हेला!”। इनमें संबोधित व्यक्ति के प्रति आत्मीयता और निकटता का भाव होता है।
- आशीर्वादबोधक – आशीर्वाद में, स्नेह से भरे ये शब्द गूंजते हैं: “दीर्घायु हो!” “जीते रहो!”। इनके माध्यम से, हमारे मन की शुभकामनाएँ और स्नेह की भावना झलकती है।
(ड़) निपात (Nipat)
निपात ऐसे शब्द होते हैं जो किसी निश्चित शब्द, शब्द समूह, या पूरे वाक्य में एक नया भाव या अर्थ जोड़ते हैं। ये अव्यय Avyay उन शब्दों के बाद लगाए जाते हैं और उनके अर्थ में एक अनूठी ताकत या प्रभाव डालते हैं। इनका काम केवल अर्थ स्पष्ट करना नहीं है; बल्कि, ये भाव को गहराई और विशिष्टता देते हैं। इसलिए निपात या अवधारक अव्यय Avyay, किसी भी वाक्य में अपनी मौजूदगी से उसे और सजीव बना देते हैं, जैसे मानो शब्दों को एक अलग ऊर्जा मिल गई हो।


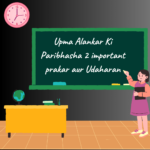
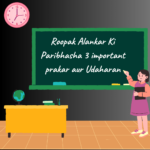


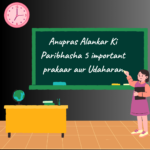
1 thought on “Avyay Ki Paribhasha, 4 important Bhed aur udaharan || Avyay Kise Kahte Hai”